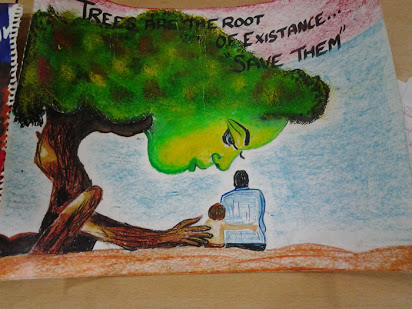अब्दुल रहीम ख़ान-ए-ख़ानाँ
अब्दुल रहीम ख़ान-ए-ख़ानाँ या सिर्फ रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे।
अब्दुल रहीम और बादशाह अकबर
जन्म :-17 दिसम्बर 1556
दिल्ली, मुगल साम्राज्य
निधन :- 1 अक्टूबर 1627 (उम्र 70)
आगरा, मुगल साम्राज्य
समाधि :- अब्दुल रहीम खान-ए-खाना का मकबरा, दिल्ली
संतान :- २
पिता :- बैरम खान
माता :- जमाल खान की बेटी
धर्म :- इस्लाम
जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किये थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती हैं। हिंदू देवी-देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहाँ भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। वे जीवनभर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवनव्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है।
छिमा बड़न को चाहिये, छोटन को उतपात।
का रहीम हरि को घट्यौ, जो भृगु मारी लात॥
जीवन परिचय संपादित करें
अबदुर्ररहीम खानखाना का जन्म संवत् १६१३ (ई. सन् १५५६) में लाहौर में हुआ था। संयोग से उस समय हुमायूँ , सिकंदर , सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे।
रहीम के पिता बैरम खाँ तेरह वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। बैरम खाँ खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमायूँ के साढ़ू और अंतरंग मित्र थे। रहीम की माँ वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खाँ की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। जब रहीम पाँच वर्ष के ही थे, तब गुजरात के पाटण नगर में सन १५६१ में इनके पिता बैरम खाँ की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन-पोषण अकबर ने अपने धर्म-पुत्र की तरह किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को 'मिर्जा खाँ' का ख़िताब दिया गया। रहीम ने बाबा जंबूर की देख-रेख में गहन अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अकबर ने अपनी धाय की बेटी माहबानो से रहीम का विवाह करा दिया। इसके बाद रहीम ने गुजरात, कुम्भलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की। इस पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि 'मीरअर्ज' से रहीम को विभूषित किया। सन १५८४ में अकबर ने रहीम को खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम का देहांत ७१ वर्ष की आयु में सन १६२७ में हुआ। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। यह मज़ार आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवनकाल में इसका निर्माण करवाया था।
अकबर के दरबार में संपादित करें
हुमायूँ ने युवराज अकबर की शिक्षा-दिक्षा के लिए बैरम खाँ को चुना और अपने जीवन के अंतिम दिनों में राज्य का प्रबंध की जिम्मेदारी देकर अकबर का अभिभावक नियुक्त किया था। बैरम खाँ ने कुशल नीति से अकबर के राज्य को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दिया। किसी कारणवश बैरम खाँ और अकबर के बीच मतभेद हो गया। अकबर ने बैरम खाँ के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया और अपने उस्ताद की मान एवं लाज रखते हुए उसे हज पर जाने की इच्छा जताई। परिणामस्वरुप बैरम खाँ हज के लिए रवाना हो गये। बैरम खाँ हज के लिए जाते हुए गुजरात के पाटन में ठहरे और पाटन के प्रसिद्ध सहस्रलिंग सरोवर में नौका-विहार के बाद तट पर बैठे थे कि भेंट करने की नियत से एक अफगान सरदार मुबारक खाँ आया और धोखे से बैरम खाँ की हत्या कर दी। यह मुबारक खाँ ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया।
इस घटना ने बैरम खाँ के परिवार को अनाथ बना दिया। इन धोखेबाजों ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया, बल्कि काफी लूटपाट भी मचाया। विधवा सुल्ताना बेगम अपने कुछ सेवकों सहित बचकर अहमदाबाद आ गई। अकबर को घटना के बारे में जैसे ही मालूम हुआ, उन्होंने सुल्ताना बेगम को दरबार वापस आने का संदेश भेज दिया। रास्ते में संदेश पाकर बेगम अकबर के दरबार में आ गई। ऐसे समय में अकबर ने अपने महानता का सबूत देते हुए इनको बड़ी उदारता से शरण दिया और रहीम के लिए कहा “इसे सब प्रकार से प्रसन्न रखो। इसे यह पता न चले कि इनके पिता खान खानाँ का साया सर से उठ गया है। बाबा जम्बूर को कहा यह हमारा बेटा है। इसे हमारी दृष्टि के सामने रखा करो। इस प्रकार अकबर ने रहीम का पालन- पोषण एकदम धर्म- पुत्र की भांति किया। कुछ दिनों के पश्चात अकबर ने विधवा सुल्ताना बेगम से विवाह कर लिया। अकबर ने रहीम को शाही खानदान के अनुरुप “मिर्जा खाँ’ की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम की शिक्षा- दीक्षा अकबर की उदार धर्म- निरपेक्ष नीति के अनुकूल हुई। इसी शिक्षा-दीक्षा के कारण रहीम का काव्य आज भी हिंदूओं के गले का कण्ठहार बना हुआ है। दिनकर जी के कथनानुसार अकबर ने अपने दीन-इलाही में हिंदूत्व को जो स्थान दिया होगा, उससे कई गुणा ज्यादा स्थान रहीम ने अपनी कविताओं में दिया। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे।
विवाह संपादित करें
रहीम की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात सम्राट अकबर ने अपने पिता हुमायूँ की परंपरा का निर्वाह करते हुए, रहीम का विवाह बैरम खाँ के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन माहबानों से करवा दिया। इस विवाह में भी अकबर ने वही किया, जो पहले करता रहा था कि विवाह के संबंधों के बदौलत आपसी तनाव व पुरानी से पुरानी कटुता को समाप्त कर दिया करता था। रहीम के विवाह से बैरम खाँ और मिर्जा के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश खत्म हो गयी। रहीम का विवाह लगभग तेरह साल की उम्र में कर दिया गया था।इनकी दस संताने थी
मीर अर्ज का पद संपादित करें
अकबर के दरबार को प्रमुख पदों में से एक मीर अर्ज का पद था। यह पद पाकर कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाता था, क्योंकि यह पद ऐसा था, जिससे पहुँचकर ही जनता की फरियाद सम्राट तक पहुँचती थी और सम्राट के द्वारा लिए गए फैसले भी इसी पद के जरिये जनता तक पहुँचाए जाते थे। इस पद पर हर दो- तीन दिनों में नए लोगों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अकबर ने इस पद का काम- काज सुचारु रूप से चलाने के लिए अपने सच्चे तथा विश्वास पात्र अमीर रहीम को मुस्तकिल मीर अर्ज नियुक्त किया। यह निर्णय सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया था। इस पद पर आसीन होने का मतलब था कि वह व्यक्ति जनता एवं सम्राट दोनों में सामान्य रूप से विश्वसनीय है।
रहीम शहजादा सलीम संपादित करें
काफी मिन्नतों तथा आशीर्वाद के बाद अकबर को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक लड़का प्राप्त हो सका, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। शहजादा सलीम माँ-बाप और दूसरे लोगों के अधिक दुलार के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन हो गया था। कई महान लोगों को सलीम की शिक्षा के लिए अकबर ने लगवाया। इन महान लोगों में शेर अहमद, मीर कलाँ और दरबारी विद्वान अबुलफजल थे। सभी लोगों की कोशिशों के बावजूद शहजादा सलीम को पढ़ाई में मन न लगा। अकबर ने सदा की तरह अपना आखिरी हथियार रहीम खाने खाना को सलीम का अतालीक नियुक्त किया। कहा जाता है रहीम यह गौरव पाकर बहुत प्रसन्न थे।
साहित्यक सृजन:
मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिन्दी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएँ प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा।
रहीम के ग्रंथो में रहीम दोहावली या सतसई, बरवै, मदनाष्ठ्क, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरवै, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवितव, सवैये, संस्कृत काव्य प्रसिद्ध हैं।
रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा “तुजके बाबरी” का फारसी में अनुवाद किया। “मआसिरे रहीमी” और “आइने अकबरी” में इन्होंने “खानखाना” व रहीम नाम से कविता की है।
रहीम व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है।
आपने स्वयं को को “रहिमन” कहकर भी सम्बोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुन्दर समावेश मिलता है।
रहीम ने अपने अनुभवों को लिस सरल शैली में अभिव्यक्त किया है वह वास्तव में अदभुत है। आपकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम ने तदभव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है।
रहीम-दास-के-दोहे, ग़ज़ब दुनिया
रहीम-दास-के-दोहे, ग़ज़ब दुनिया
रहीम के दोहे –
दोहा : दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय ।
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख काहे होय ।
भावार्थ : संकट में हर कोई प्रभु को याद करता है खुशी में कोई नहीं, अगर आप खुशी में भी याद करते तो संताप होता ही नही ।
दोहा : जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाहिं ।
गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुःख मानत नाहिं ।
भावार्थ : रहीम दास कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े की भव्यता कम नहीं होती, क्योंकि गिरधर को कन्हैया कहने से उनके गौरव में कमी नहीं होती ।
दोहा : रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि ।
जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारि ।
भावार्थ : रहीम दास कहते हैं कि बड़ी चीजों को देखते हुए, छोटी चीजों को फेंक देना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां छोटी सुई का इस्तेमाल किया जाता है, वहां बड़ी कृपाण क्या कर सकती है? मतलब हर चीज़ का अपना एक अनोखा मोल, उपयोग होता है । कोई भी चीज़ न बड़ी होती है और न ही छोटी होती है ।
दोहा : रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय ।
टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाय ।
भावार्थ : रहीम दास ने कहा है कि प्रेम का संबंध बहुत नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता । यदि यह धागा एक बार टूट जाता है, तो इसे जोड़ना मुश्किल होता है, और अगर यह जुड़ भी जाता है तो बीच में गांठ बन जाती है । ठीक वैसे ही आपसी संबंध टूट जाने पर जुड़ते नहीं और जुड़ते है तो भी मन में एक दरार सी हो जाती है ।
दोहा : रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार ।
रहिमन फिरि-फिरि पोइए, टूटे मुक्ताहार ।
भावार्थ : यदि हार टूट जाये तो उन हीरो को धागे में पीरों लेना चाहिये, वैसे ही यदि आपके प्रियजन आपसे सौ बार भी रूठे तो उन्हें मना लेना चाहिये ।
दोहा : दोनों रहिमन एक से, जों लों बोलत नाहिं ।
जान परत हैं काक पिक, रितु बसंत के माहिं ।
भावार्थ : रहीम दास का कहना है कि काग और कोयल समान रूप से काले रंग के होते हैं । जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती तब तक उनकी पहचान नहीं होती है, लेकिन जब बसंत ऋतु आ जाती है, तो दोनों के बीच का अंतर कोयल की मीठी सुरीली आवाज से प्रकट हो जाता है ।
दोहा : बानी ऐसी बोलिये, मन का आपा खोय ।
औरन को सीतल करै, आपहु सीतल होय ।
भावार्थ : अपने भीतर के दंभ को दूर करके ऐसी मीठी बातें करनी चाहिए जिसे श्रवण कर के खुद को और दूसरों को शांति और ख़ुशी हो ।
दोहा : जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग ।
चन्दन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग ।
भावार्थ : रहीम दास ने कहा है कि जो लोग अपनी प्रकृति में अच्छे हैं वे खराब संगती में भी खराब नहीं हो सकते हैं, जैसे विषैले सर्प सुगंधित चंदन के वृक्षों को लिपटे रहते है फिर भी चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक वैसे ही ।
दोहा : समय पाय फल होत है, समय पाय झरी जात ।
सदा रहे नहिं एक सी, का रहीम पछितात ।
भावार्थ : रहीम दास कहते हैं कि कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, जैसा कि जब वसंत आती है तो पेड़ पर फल लगते है और जब शरद आती है तो सब गिर जाता है इसलिए विकट स्थिति में पछताना व्यर्थ है ।
दोहा : वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग ।
बांटन वारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग ।
भावार्थ : रहीम कहते हैं कि धन्य है वो लोग जिनका जीवन सदा परोपकार के लिए बीतता है, जिस तरह फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है ठीक वैसे ही इन परोपकारियों का जीवन भी खुश्बू से महकता रहता है ।
दोहा : खीरा सिर ते काटि के, मलियत लौंन लगाय ।
रहिमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाय ।
भावार्थ : रहिम दास जी कहते हैं कि खीरे के कड़वाहट को दूर करने के लिए, इसके ऊपरी छोर को काटने के बाद उस पर लोन (नमक) लगाया जाता है। यह सजा उन लोगों के लिए सही है जो कड़वा शब्द कहते हैं।
दोहा : रहिमन अंसुवा नयन ढरि, जिय दुःख प्रगट करेइ ।
जाहि निकारौ गेह ते, कस न भेद कहि देइ ।
भावार्थ : : आँसू आँख से बाहर निकलते हैं और दिमाग की पीड़ा प्रकट करते हैं, रहीम दास कहते है कि ठीक वैसे ही घर से निकाला गया ही घर के भेद खोलेगा ।
दोहा : रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय ।
सुनी इठलैहैं लोग सब, बांटी न लेंहैं कोय ।
भावार्थ : रहीम दास कहते हैं कि आपके मन की उदासी को अपने मन के भीतर ही छुपाये रखे, क्योंकि दूसरों की उदासी को सुनने के बाद लोग इठला भले ही लेते है लेकिन उसे बाँट कर कम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं ।
दोहा : तरुवर फल नहीँ खात हैं, सरवर पियहि न पान ।
कही रहीम पर काज हित, संपति संचही सुजान ।
भावार्थ : पेड़ अपने फल-फूल स्वयं नहीं खाते हैं, और नदियाँ भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं । उसी प्रकार सज्जन लोग वे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, दान के काम के लिए अपने धन दौलत को खर्च करते हैं ।
दोहा : जे गरिब सों हित करें, ते रहीम बड़ लोग ।
कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग ।
भावार्थ : : जो लोग गरीब के हित में हैं, बड़े महान लोग हैं । जैसे सुदामा कहते हैं कि कान्हा की मैत्री भी एक भक्ति है ।
दोहा : रहिमन विपदा हू भली, जो थोरे दिन होय ।
हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय ।
भावार्थ : रहीम कहते हैं कि संघर्ष जरूरी है क्योंकि इस समय के दौरान ही यह ज्ञात होता है कि हमारे हित में कौन है और अहित में कौन है ।
दोहा : बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ।
भावार्थ : बड़ा होना इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के लिए अच्छा है । जैसे खजूर के पेड़ की तरह, वो बहुत बड़ा है लेकिन इसके फल इतनी दूर है कि इसे तोड़ना मुश्किल है और काफिर को छाँव के काम भी नहीं आता ।
दोहा : रहिमन चुप हो बैठिये, देखि दिनन के फेर ।
जब नीके दिन आइहैं, बनत न लगिहैं देर ।
भावार्थ : रहीम दास कहते है कि जब ख़राब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही ठीक, क्योंकि जब अच्छा समय आता हैं तब काम बनते विलंब नहीं होता इसलिए हमेशा अपने सही समय का सब्र करे ।
दोहा : मन मोटी अरु दूध रस, इनकी सहज सुभाय ।
फट जाये तो न मिले, कोटिन करो उपाय ।
भावार्थ : रस, फूल, दूध, मन और मोती जब तक स्वाभाविक सामान्य रूप में है तब तक अच्छे लगते है लेकिन यह एकबार टूट-फट जाए तो कितनी भी युक्तियां कर लो वो फिर से अपने स्वाभाविक और सामान्य रूप में नहीं आते ।
दोहा : बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय ।
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय ।
भावार्थ : रहीम दास कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण से कुछ गलत हो जाता है, तो इसे सही करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार दूध खराब हो जाये, तो हजार कोशिश कर ले उसमे से न तो मक्खन बनता है और न ही दूध ।
दोहा : जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह ।
धरती ही पर परत है, सीत घाम औ मेह ।
भावार्थ : रहीम दास कहते हैं कि जैसे इस धरती पर सर्दी, गर्मी और बारिश गिरती है और जैसे यह सब पृथ्वी सहन करती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर को भी सुख और दुख उठाना और सहना सीखना चाहिए ।
दोहा : ओछे को सतसंग रहिमन तजहु अंगार ज्यों ।
तातो जारै अंग सीरै पै कारौ लगै ।
भावार्थ : नीच लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनसे हर स्तर पर, हमें क्षति ही होती है । जैसे जब कोयला गर्म होता है तब तक शरीर को जलाता है और जब ठंडा हो जाता है, तो शरीर को काला करता है ।
दोहा : रहिमन मनहि लगाईं कै, देख लेहूँ किन कोय ।
नर को बस करिबो कहा, नारायण बस होय ।
भावार्थ : रहिम दास कहते हैं कि यदि आप अपने मन को एक स्थान पर रखकर काम करेंगे, तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, अगर मनुष्य एक मन से ईश्वर को चाहे तो वह ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है ।
भाषा शैली संपादित करें
रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है।
यह रहीम निज संग लै, जनमत जगत न कोय।
बैर, प्रीति, अभ्यास, जस, होत होत ही होय ॥
उनके काव्य में शृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवै, कवित्त और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीम दास जी की भाषा अत्यंत सरल है, उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुन्दर समावेश मिलता है। उन्होंने सोरठा एवं छंदों का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य रचनाओं को किया है| उन्होंने ब्रजभाषा में अपनी काव्य रचनाएं की है| उनके ब्रज का रूप अत्यंत व्यवहारिक, स्पष्ट एवं सरल है| उन्होंने तदभव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य भाषाओं का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है| अवधी के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी रहीमजी ने अपनी रचनाओं में किया है, उनकी अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में की गई हैं जो कि अत्यंत ही सरल एवं बोधगम्य है |
प्रमुख रचनाएं संपादित करें
रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि।